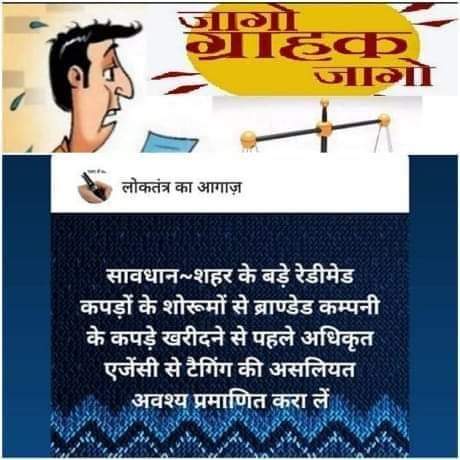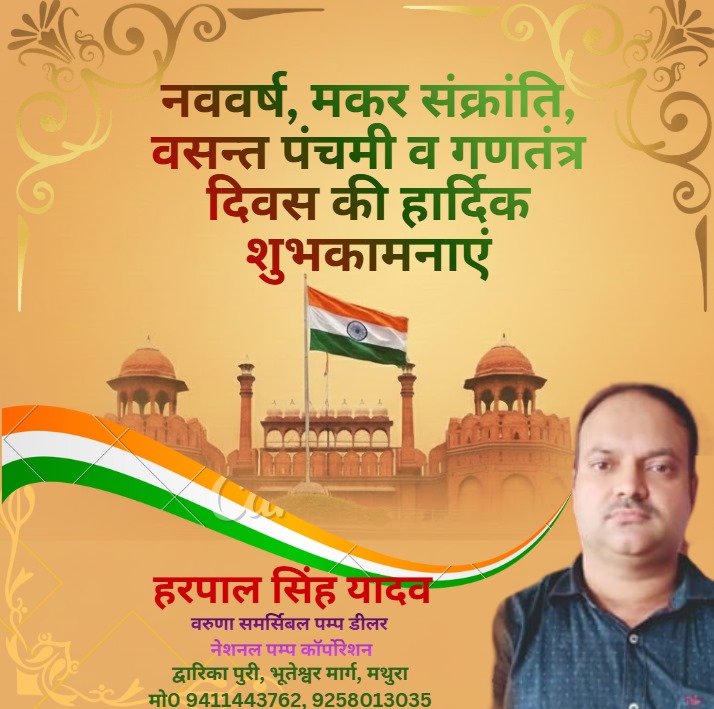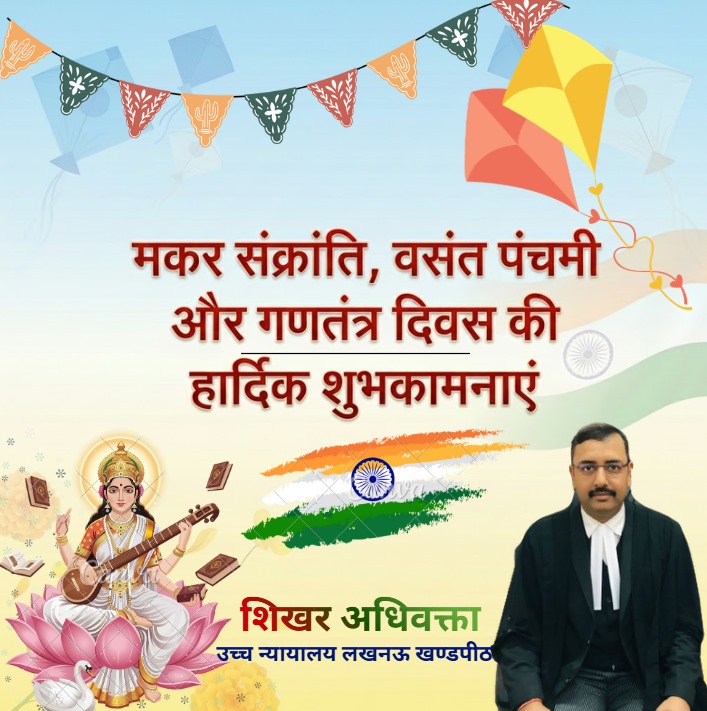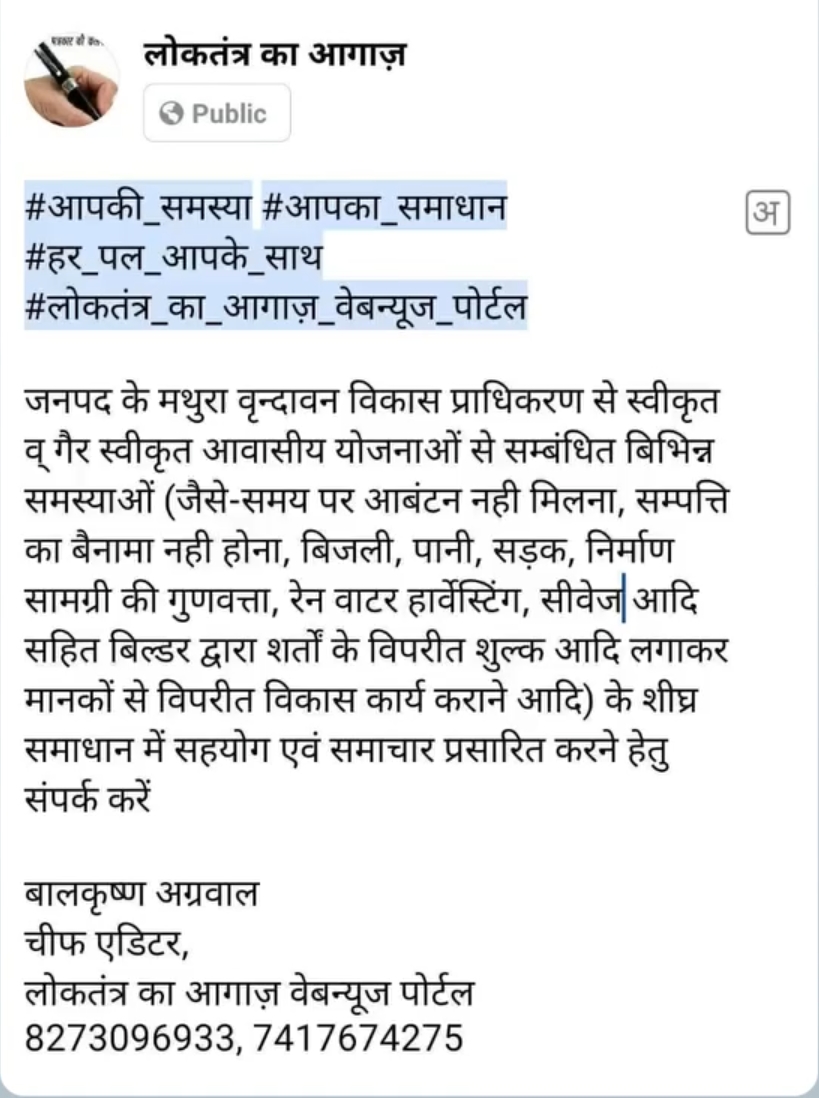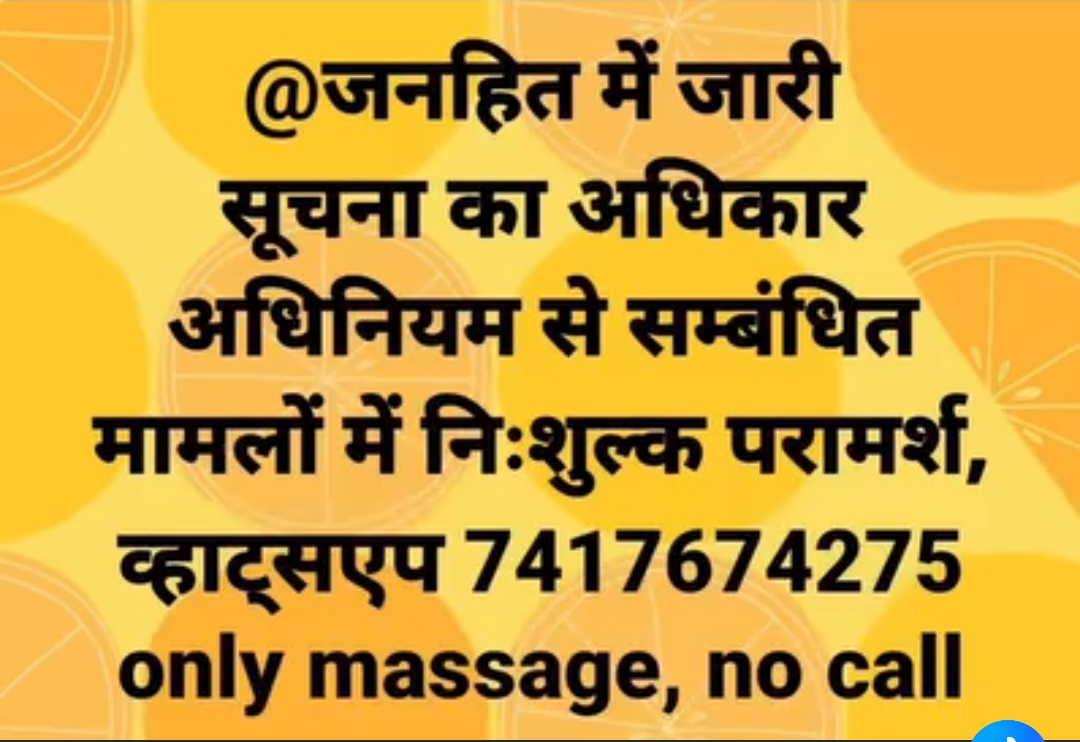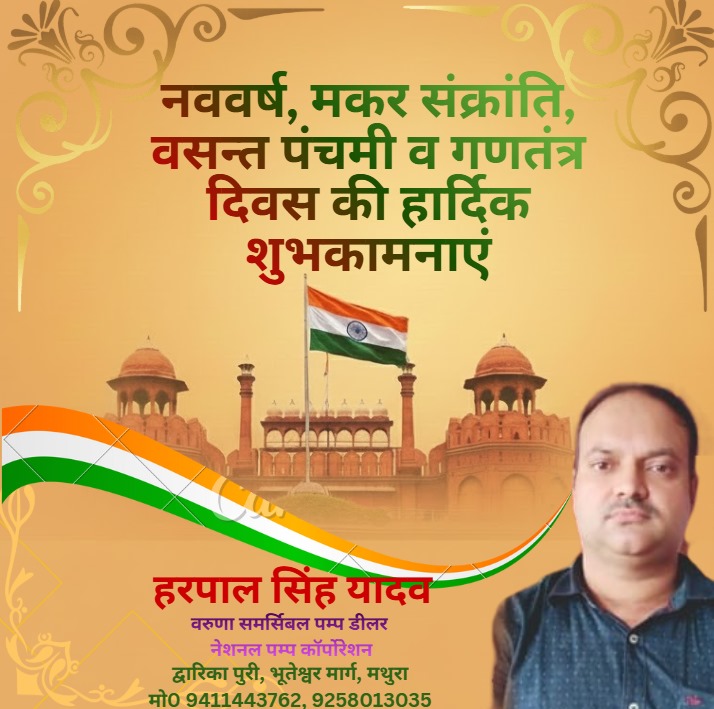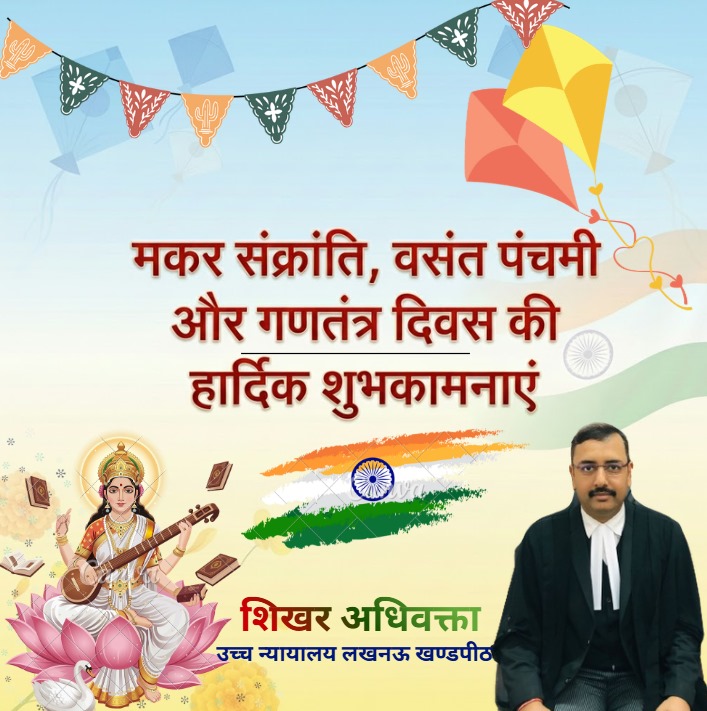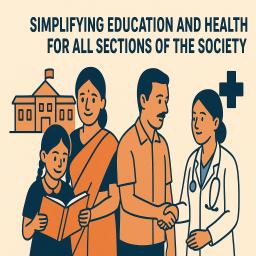
भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को हर वर्ग के लिए आसान बनाने के उपाय
भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को हर वर्ग के लिए आसान बनाने के उपाय
स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की रीढ़ होती हैं, ये ना केवल व्यक्तिगत उन्नति के साधन हैं बल्कि राष्ट्र की उत्पादकता, समानता और स्थिरता के प्रमुख स्तंभ भी हैं, भारत जैसे विशाल और विविधता-पूर्ण देश में यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति—चाहे अमीर हो या गरीब, ग्रामीण हो या शहरी—इन मूलभूत सुविधाओं तक समान पहुँच रखे, एक बड़ी चुनौती है, हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) और 21-A (शिक्षा के अधिकार) ने इन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, परंतु व्यवहार में सामाजिक-आर्थिक विषमता के कारण इन सेवाओं की पहुँच अब भी असमान है ।
.jpg)
1. वर्तमान परिदृश्य — असमान पहुँच की सच्चाई
(क) स्वास्थ्य क्षेत्र में असमानता
@ ग्रामीण भारत में आज भी लगभग 60% आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ पर्याप्त रूप से नहीं मिलतीं ।
@ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर-मरीज अनुपात बहुत कम है, वहीं निजी अस्पताल गरीबों की पहुँच से बाहर हैं ।
@ स्वास्थ्य पर होने वाला व्यक्तिगत खर्च भारत में लगभग 50% से अधिक है जिससे गरीब परिवार आर्थिक रूप से टूट जाते हैं।
(ख) शिक्षा क्षेत्र में असमानता
@ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में विद्यालयों की संख्या तो है, पर शिक्षक, संसाधन और गुणवत्ता का भारी अभाव है ।
@ निजी स्कूलों की फीस आम वर्ग की पहुँच से बाहर होती जा रही है ।
@ उच्च शिक्षा में प्रवेश, अनुसंधान और रोजगार-मुखी शिक्षा तक पहुँच भी वर्ग विशेष तक सीमित है।
.jpg)
2. क्यों आवश्यक है सभी के लिए समान सहूलियत
A. सामाजिक न्याय का आधार- जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे, तभी समाज में समानता और न्याय संभव है।
B. आर्थिक प्रगति -शिक्षित और स्वस्थ जनशक्ति ही उत्पादक श्रमशक्ति बनती है, जिससे जीडीपी वृद्धि तेज होती है।
C. गरीबी उन्मूलन — स्वास्थ्य खर्च घटाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से गरीब वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बनता है।
D. लोकतंत्र की मज़बूती — जब नागरिक शिक्षित और जागरूक होंगे, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
.jpg)
3. स्वास्थ्य को सभी वर्गों के लिए आसान बनाने के उपाय
(क) प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचे को सशक्त बनाना
@ हर गाँव और वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र, और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स स्थापित की जाएँ।
@स्थानीय स्तर पर नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए।
(ख) स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त इलाज की सार्वभौमिक पहुँच
@ आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाए ताकि हर नागरिक, चाहे वह BPL कार्डधारक हो या नहीं, बुनियादी इलाज मुफ्त पा सके।
@निजी अस्पतालों को भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जोड़कर गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
(ग) दवाओं और जाँचों की सस्ती उपलब्धता
@ जन औषधि केंद्रों की संख्या हर जिले और तहसील में बढ़ाई जाए।
@ सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाइयाँ और पैथोलॉजी परीक्षण मुफ्त या न्यूनतम दर पर उपलब्ध हों।
(घ) स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण और टेली-मेडिसिन
@दूरदराज़ क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए e-Sanjeevani जैसी टेली-कंसल्टेशन सेवाएँ बढ़ाई जाएँ।
@ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और हेल्थ-आईडी के माध्यम से रोगियों की जानकारी सुरक्षित रखी जाए।
(ड़) स्वास्थ्य शिक्षा और जनजागरूकता
@ स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषय अनिवार्य किए जाएँ।
@ पंचायत और नगर निकाय स्तर पर नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित हों।
.jpg)
4. शिक्षा को सबके लिए आसान और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उपाय
(A) समान अवसर वाली शिक्षा नीति
सरकारी और निजी स्कूलों के बीच गुणवत्ता-अंतर को कम किया जाए।
(B) सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण
@डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय जैसी सुविधाएँ हर सरकारी विद्यालय में हों।
@शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर किया जाए तथा शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
(C) गरीब वर्ग के लिए वित्तीय सहायता
@ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को फीस माफी, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट दी जाए।
@ निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार के तहत 25% सीट आरक्षित रखी जाएँ और इसका कठोर पालन हो।
(D) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार
@युवाओं को उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
@ आईटीआई , पॉलिटेक्निक और स्किल डेवलपमेंट सेंटर गाँव-गाँव तक पहुँचाए जाएँ।
(E) डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट सुलभता
@ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट सुविधा और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
@“एक भारत डिजिटल शिक्षा मिशन” जैसे कार्यक्रम से हर बच्चे को ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच मिले।
5. सरकारी-सामाजिक साझेदारी का मॉडल
(1) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप—निजी संस्थाओं की दक्षता और सरकार की नीतिगत शक्ति का संयोजन।
(2) एनजीओ और सामुदायिक भागीदारी — स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ स्वास्थ्य-शिक्षा अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
(3) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीसीआर ) — निजी कंपनियाँ अपने सीसीआर बजट से ग्रामीण स्कूलों और अस्पतालों को सहयोग दें।
(4) सामाजिक ऑडिट — हर जिले में नागरिक समितियाँ बनाई जाएँ जो यह देखें कि सरकारी योजनाएँ लाभार्थियों तक सही पहुँच रही हैं या नहीं।
6. दीर्घकालिक दृष्टिकोण
@ मानव पूंजी निवेश नीति: सरकार जीडीपी का न्यूनतम 6% शिक्षा पर और 3% स्वास्थ्य पर खर्च करे।
@राज्य स्तर पर क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने की नीति: पिछड़े जिलों को अतिरिक्त फंडिंग दी जाए।
@शहरी-ग्रामीण संतुलन: बड़े शहरों के साथ ग्रामीण और जनजातीय इलाकों पर समान ध्यान दिया जाए।
@ पारदर्शिता और जवाबदेही: हर योजना का ऑनलाइन डेटा, बजट उपयोग और परिणाम सार्वजनिक किया जाए।
निष्कर्ष : भारत की सच्ची प्रगति तब होगी जब हर नागरिक—जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आय स्तर से परे—स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा अवसरों तक समान पहुँच रखेगा। यह केवल सरकारी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है, सस्ती दवाइयाँ, सुलभ अस्पताल, डिजिटल शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और जनभागीदारी—ये पाँच स्तंभ ऐसे भारत की नींव रख सकते हैं जहाँ “सबका स्वास्थ्य, सबकी शिक्षा” केवल नारा नहीं, बल्कि वास्तविकता बने।
शिखर अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ।



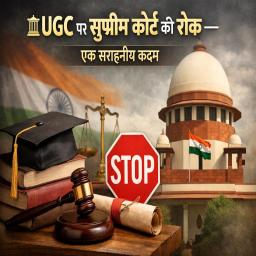
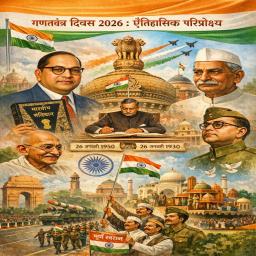











.jpeg)